ज्योतिष प्रवेशिका (Jyotish Praveshika) “ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणाम् बोधकं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम्” के अनुसार सूर्यादि ग्रह एवं काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिषशास्त्र कहा गया है। इसमें प्रमुख रूप से ग्रह, नक्षत्र, तारागण, धूमकेत्वादि ज्योतिपदार्थों के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, पथ व काल, ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति व इनके संचरण के आधार पर शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। भारतीय मनीषियों की सर्वप्रथम दृष्टि सूर्य एवं चन्द्रमा पर पड़ी थी। उन्होंने इनसे अभिभूत होकर इन्हें देवत्वरूप में मान लिया था। इसका स्पष्ट प्रमाण वैदिक साहित्य में जगह-जगह पर सूर्य एवं चन्द्रमा से सम्बधित स्तुतिपरक मन्त्रों से प्राप्त होता है। बाद में ब्राह्मण व अरण्यक काल में परिभाषा का स्वरूप बदलता पाया गया है।
उस काल में नक्षत्रों की आकृति, स्वरूप, गुण व प्रभाव का परिज्ञान करना ज्योतिष का स्वरूप माना जाने लगा। प्रारम्भिक काल में नक्षत्रों के शुभाशुभ कालानुसार कार्यों का विवेचन तथा ऋतु, अयन, दिनमान, लग्नादि के शुभाशुभ के अनुसार करणीय कार्यों को करने का ज्ञान प्राप्त करना भी ज्योतिष शास्त्र की पारिभाषिक परिधि में समाहित हो गया। आदिकाल के अन्त में ज्योतिष के गणित व फलित ये दोनों भेद स्वतन्त्र रूप में विकसित हो चुके थे। ग्रहों की गति, स्थिति व अयनांश आदि गणित स्कन्ध में था और शुभाशुभ समय का निर्णय आदि विधायक कार्यों के लिए समय व स्थानादि का निर्धारण फलित स्कन्ध में माना जाने लगा। मध्यकाल में अर्थात् ईस्वीय सन् ५०० से १००० के बीच सिद्धान्त ज्योतिष के स्वरूप का और विकास हुआ। इस काल में ज्योतिषशास्त्र का स्कन्धत्रय में विभाजन हो गया। इसका सिद्धान्त, संहिता और होरा के रूप में विकास हुआ। आगे चलकर इसमें दो संशोधन और विकसित हुए।
यह पंचरूपात्मक हो गया इसमें प्रश्न एव निमित्त दो रूप और जुड़ गये। अहोरात्र का संक्षिप्त रूप होरा कहलाता है। इसमें जन्म कुण्डली के द्वादश भावों का फल, उनमें स्थित ग्रहों की स्थिति एवं दृष्टि के अनुसार फलों का निर्धारण प्रारम्भ हुआ। मानव जीवन के सुख-दुःख, इष्ट-अनिष्ट, उन्नति-अवनति तथा भाग्योदय आदि शुभा-शुभ का वर्णन या निर्धारण इसके द्वारा किया जाने लगा। होरा ग्रन्थों में भी फलनिरूपण के दो प्रकार हैं। एक में जन्म नक्षत्र पर आधारित एवं दूसरे में जन्म लग्न पर आधारित द्वादश भावों के फल कथन की प्रणाली प्रचलित हो गयी। होरा शास्त्रों में भी अनेक परिवर्तन व संशोधन विकसित हुए। प्रमुख रूप से इन शास्त्रों के रचयिता वराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्धसेन, दुण्ढ़िराज एवं केशव आदि हैं। राशियों के स्वरूपानुसार भाव व दृष्टि का समन्वय करके कारक व मारक ग्रहविशेषों के फलप्रतिपादन की प्रक्रिया नारचन्द्र ने आरम्भ की। श्रीपति व श्रीधर आदि ने नवीं व दशवीं शताब्दी में ग्रहवल, ग्रहवर्ग, विंशोत्तरी आदि दशाओं पर फल-प्रतिपादन की प्रणाली विकसित की।





![Jyotish Praveshika (ज्योतिष प्रवेशिका)[BVP] 1 bvs0094 1](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/bvs0094_1-300x300.jpg)
![Jyotish Praveshika (ज्योतिष प्रवेशिका)[BVP] 2 7f9cb267 0fc1 452d bf25 c3e4d3911ec4](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/7f9cb267-0fc1-452d-bf25-c3e4d3911ec4-300x300.jpg)
![Jyotish Praveshika (ज्योतिष प्रवेशिका)[BVP] 3 bff2c6b3 2ac2 48ef bcff 07b1fd1ab6c3](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/bff2c6b3-2ac2-48ef-bcff-07b1fd1ab6c3-300x300.jpg)
![Jyotish Praveshika (ज्योतिष प्रवेशिका)[BVP] 4 6c72bb9d bf3f 44e3 966f f80325f1cdfe](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/6c72bb9d-bf3f-44e3-966f-f80325f1cdfe-300x300.jpg)
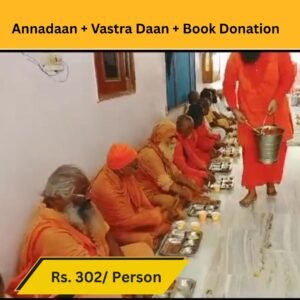


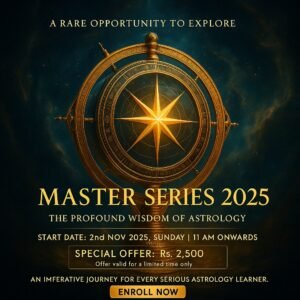

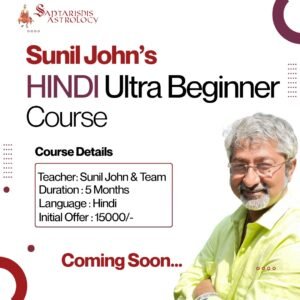



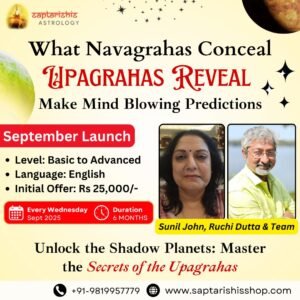


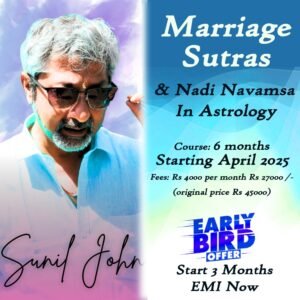
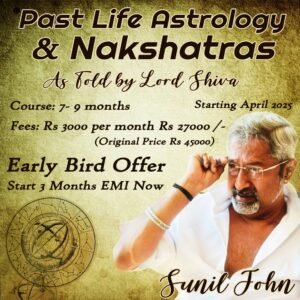
![Brihad Vakahdachakram Paperback [BVP] 5 db86bad5 db96 4566 9785 b57f311274f1](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/db86bad5-db96-4566-9785-b57f311274f1-100x100.jpg)
![Ketaki Grah Ganitam (केतकिग्रहगणितम्) [BVP] 6 TBVP0219 1](https://saptarishisshop.com/wp-content/uploads/2025/03/TBVP0219_1-100x100.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.